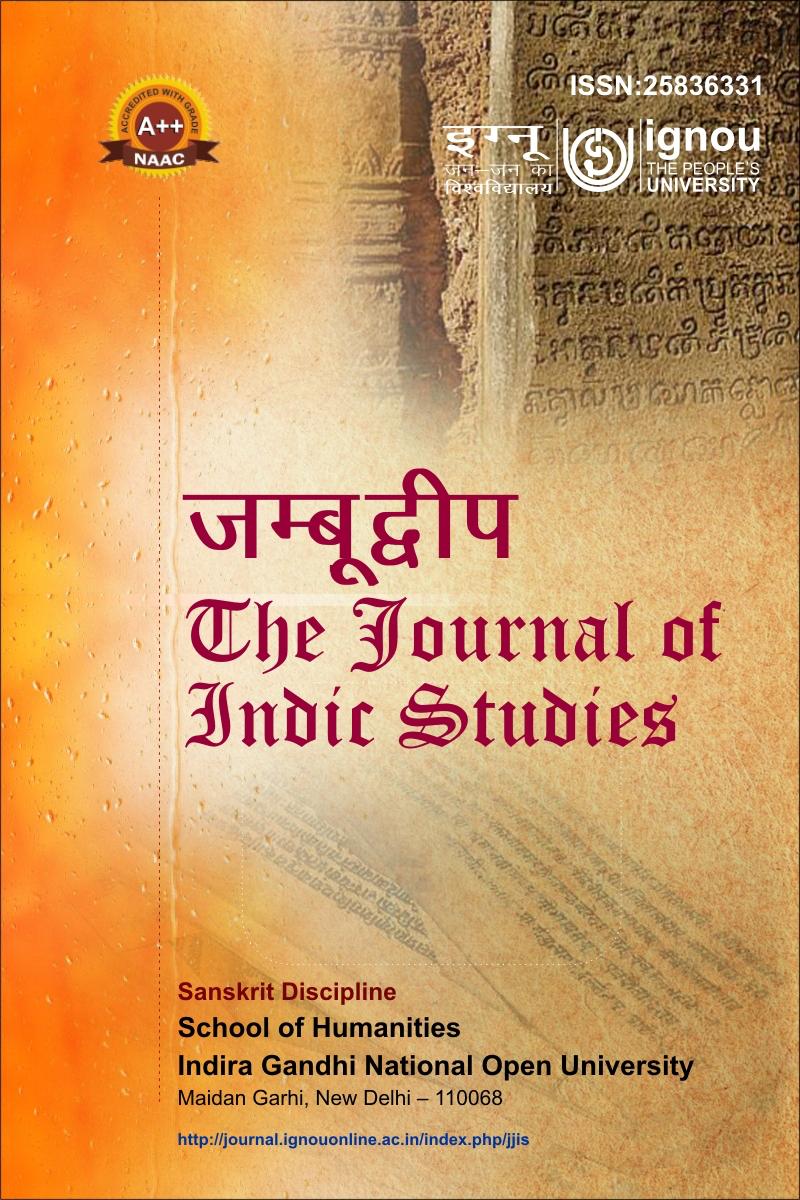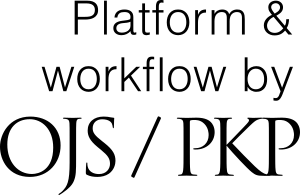सांख्यदर्शन: पातञ्जलयोग तथा बौद्ध योग का मूलस्रोत
-
Abstract
-शोध सारांश
भारतीय दर्शन की विविध धाराएँ आत्मज्ञान, मुक्ति और मानव दु:ख की गहन व्याख्या करती
हैं।वेद, उपनिषद्और विभिन्न दर्शनों (सांख्य, योग, वेदांत आदि) में इन प्रश्नों को भिन्न दृष्टिकोणों
से संबोधित किया गया है। विशेष रूप से, बौद्धदर्शन औरयोगदर्शन ने भारतीय चिंतन परंपरा
को न केवल आकार दिया है, अपितु व्यावहारिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। इनमें गौतम बुद्ध
और महर्षि पतञ्जलि विशेष स्थान रखते हैं।
यद्यपि गौतम बुद्ध और महर्षि पतञ्जलि अलग-अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों से आते हैं-एक
श्रमण परंपरा से और दूसरा वैदिक परंपरा से परंतु फिर भी दोनों की शिक्षाओं में आश्चर्यजनक
साम्य देखने को मिलता है। इस साम्यता की जड़ें कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन में
निहित हैं, जिसे योग तथा बौद्ध परंपरा दोनों ने अपने-अपने तरीके से आत्मसात किया है।
उनकेदृष्टिकोणोंमेंकईबाह्यअंतरदिखाईदेतेहैं, परंतु सूक्ष्म अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि दोनों
की शिक्षाओं की जड़ें एक समान दार्शनिक आधारमें निहित हैं। यह दर्शन, चेतना और भौतिक
प्रकृति के द्वैत पर आधारित है, जो पतञ्जलि के योगसूत्रों और बुद्ध के मध्यम मार्ग दोनों में
गहराई से प्रतिबिंबित होता है।विशेषतः कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित पुरुष–प्रकृति द्वैतवाद, दुख की उत्पत्ति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषणऔर कैवल्य की अवधारणा ने पतंजलि और बुद्ध,
दोनों को प्रभावित किया।
यद्यपि उन्होंनेअलग-अलग सांस्कृतिक और दार्शनिक मार्ग अपनाए, परंतुउनकाउद्देश्यएकहीरहा-
मानव दु:ख से मुक्ति।उनकी शिक्षाएँ आज भी ध्यान, योग और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।इस प्रकार, सांख्य दर्शन को पातञ्जल योग और बौद्ध योग का
मूलस्रोत कहना न केवल तर्क संगतहै, बल्कि यह भारत की दार्शनिक एकता और विविधता का
जीवंत प्रमाण भी है।
कूट शब्द:सांख्य दर्शन, पातञ्जल योग, बौद्ध दर्शन, प्रकृति, पुरुष, कैवल्य