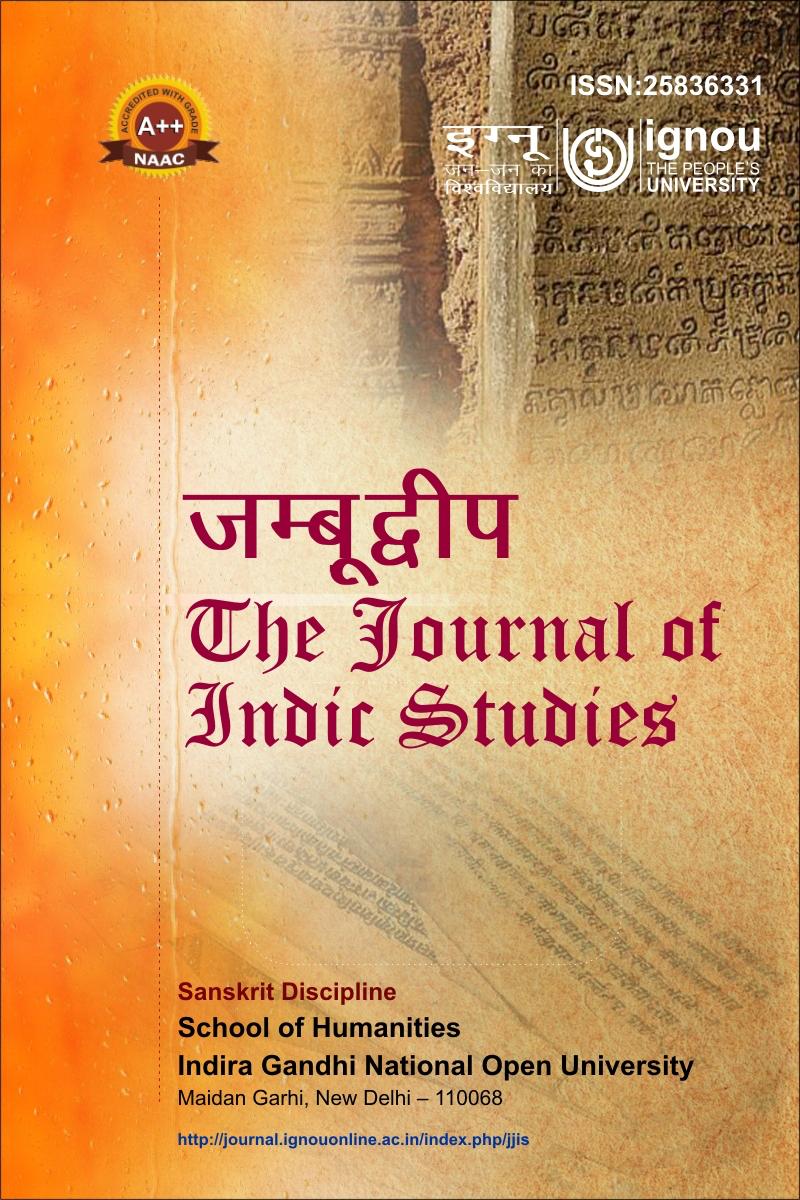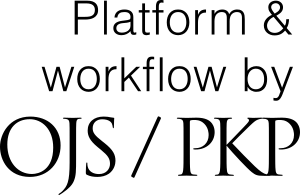वास्तुशास्त्र मे प्रतिमालक्षण
वास्तुशास्त्र में प्रतिमालक्षण
Abstract
शोधसारांश- वास्तुशास्त्र में प्रतिमालक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है जो भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिक
परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रतिमालक्षण का तात्पर्य मूर्तियों और देवप्रतिमाओं के निर्माण और उनके
स्थापत्य के नियमों से है, जो वास्तुकला और मूर्तिकला में समुचित संतुलन और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। प्रतिमा
न केवल एक धार्मिक प्रतीक होती है, बल्कि उसमें शिल्प और सौंदर्य का समन्वय भी होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया
वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, और सौंदर्यशास्त्रीय मान्यताओं को
ध्यान में रखते हुए प्रतिमा का निर्माण करती है।किसी भी प्रतिमा का निर्माण केवल सौंदर्य और आकार पर आधारित
नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे शास्त्रों में वर्णित गुणों और मानकों का पालन करना आवश्यक है। इसमें प्रतिमा के
आकार, अनुपात, मुद्रा, चेहरे के भाव, और उसकी संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए,
देवताओं की मूर्तियों में उनके आध्यात्मिक गुणों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से मुखाकृति, नेत्र, और हस्त
मुद्राओं का महत्व होता है। शिव, विष्णु, दुर्गा, और अन्य देवताओं की प्रतिमाओं में उनकी शक्ति और स्वभाव को
मूर्तरूप देने के लिए उनके अंग-प्रत्यंगों का विशिष्ट वर्णन शास्त्रों में किया गया है।
प्रतिमाओं के निर्माण में सामग्री का भी विशेष महत्व होता है। शिल्पकारों को विभिन्न धातुओं, पत्थरों, और
लकड़ियों के माध्यम से प्रतिमा निर्माण करना होता है, और यह सामग्री भी वास्तुशास्त्र के अनुसार चुनी जाती है।
प्रत्येक सामग्री का अपना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है, और यह प्रतिमा की ऊर्जा और उसकी पूजा के
उद्देश्य से मेल खाती है। जैसे कि विष्णु की प्रतिमा को शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ दिखाया जाता है, जिससे
उनकी दिव्य शक्तियों का प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन होता है।
वास्तुशास्त्र में प्रतिमा की ऊँचाई और अनुपात का भी स्पष्ट उल्लेख है। शरीर के प्रत्येक अंग का विशेष माप होता है,
जो मूर्ति के सौंदर्य और संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इस माप में अंगों का विस्तार, उनकी
दूरी, और शरीर के विभिन्न हिस्सों का सही संतुलन महत्वपूर्ण होता है। उदाहरणस्वरूप, हाथ की लंबाई, पैर की
लंबाई, मुख का आकार, और आँखों की स्थिति जैसी सूक्ष्म बातें भी शास्त्रों में विस्तार से वर्णित की गई हैं।इसके
अतिरिक्त, प्रतिमालक्षण में प्रतिमा की मुद्रा (आसन) भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। मूर्तियों की अलग-अलग मुद्राएँ
उनके द्वारा धारण किए गए विशेष गुणों और भावनाओं को दर्शाती हैं। जैसे कि ध्यान मुद्रा में बैठी बुद्ध की प्रतिमा
उनके शांति और ध्यान के गुणों को प्रस्तुत करती है, वहीं नटराज रूप में शिव की प्रतिमा उनके तांडव नृत्य के
माध्यम से सृष्टि और संहार के चक्र का प्रदर्शन करती है। इसी प्रकार, लक्ष्मी की प्रतिमा में उन्हें धन और समृद्धि की
देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें वे हाथों से आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में होती हैं।
वास्तुशास्त्र में प्रतिमालक्षण का मुख्य उद्देश्य देवताओं के प्रतीक रूपों को इस प्रकार से तैयार करना है कि वे न केवल
आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें, बल्कि उस देवता की उपासना और आराधना में सहायक बनें। इसके साथ ही,
प्रतिमाओं के निर्माण में वास्तुशास्त्र यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें उनके स्थापन स्थल के अनुरूप स्थापित किया
जाए, जिससे वह स्थान सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो सके और भक्तों को आध्यात्मिक शांति और संतोष प्राप्त
हो।प्रतिमालक्षण के इन सिद्धांतों का पालन करने से वास्तु और मूर्तिकला के क्षेत्र में उच्च कोटि की रचनाएँ देखने को
मिलती हैं, जो भारतीय संस्कृति और धर्म का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।