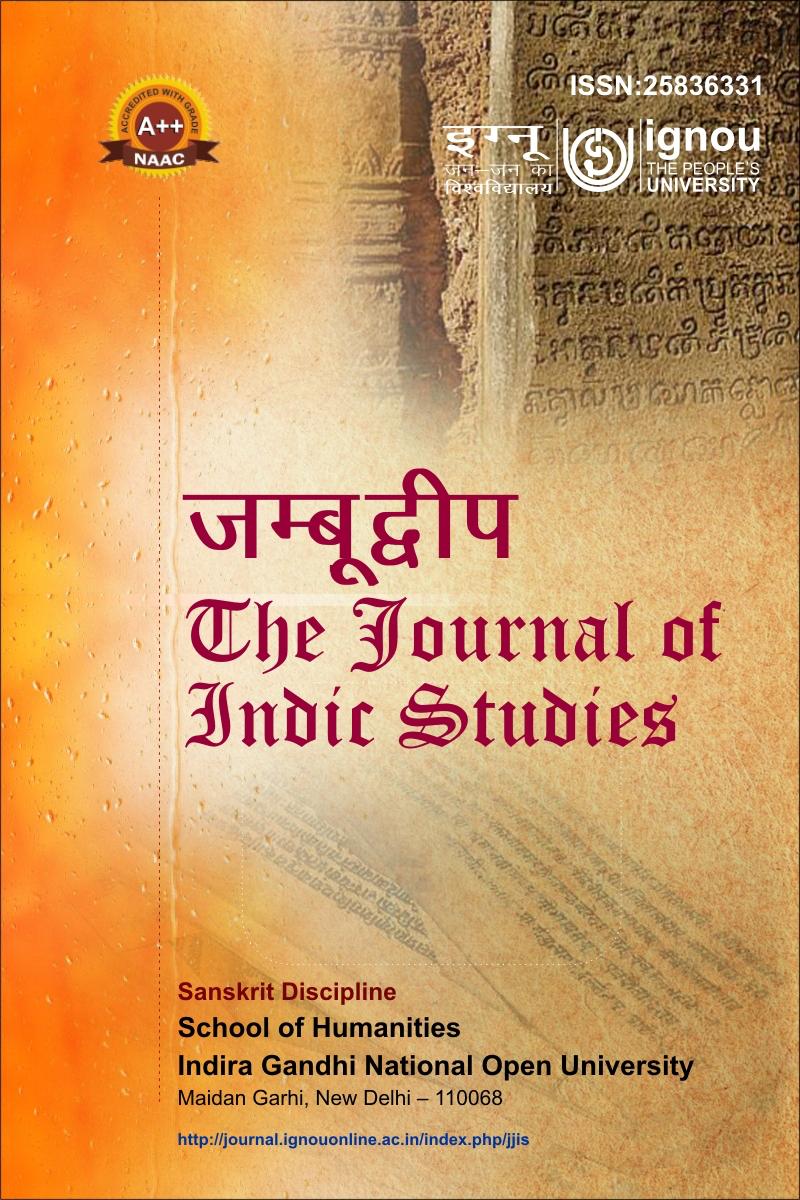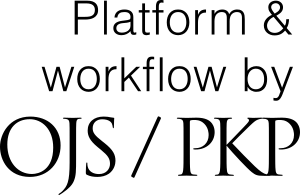औपनिवेशिक विज्ञान और भारतीय गणित: महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के परिप्रेक्ष्य में
Abstract
शोध सारांश
उन्नीसवीं सदी में किए गए भारतीय महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण (Great Trigonometrical Survey of India) (जिसे आगे जीटीएसआई/GTSI कहा जाएगा) को अक्सर औपनिवेशिक आख्यानों में यूरोपीय विज्ञान और संगठन की एक अद्वितीय उपलब्धि के रूप में सराहा जाता है। हालाँकि, ऐसे विवरण इस विशाल उद्यम और त्रिकोणमिति, खगोल विज्ञान और भूमि मापन की दीर्घकालिक भारतीय परंपराओं के बीच गहरेसंबंधों को अस्पष्ट कर देते हैं। जीटीएसआई (GTSI) से बहुत पहले, सिद्धांत काल से लेकर अंतर-महाद्वीपीय मध्ययुगीन आदान-प्रदान तक, भारतीय गणितज्ञों ने ज्या, स्पर्श रेखा और खगोलीय स्थितियों की गणना के लिए परिष्कृत विधियाँ विकसित की थीं, जिनसे व्यावहारिक सर्वेक्षण और सैद्धांतिक गणना दोनों को जानकारी मिली। यह अध्ययन स्वदेशी गणितीय विरासत के दृष्टिकोण से पुनर्मूल्यांकन करता है, और औपनिवेशिक वैज्ञानिक व्यवहार की विशेषता वाले ज्ञानात्मक अंतःक्रियाओं, अनुकूलनों और कभी-कभी विनियोगों का पता लगाता है।शोधपत्र में तर्क दिया गया है कि जीटीएसआई (GTSI) एक विच्छेद नहीं, बल्कि विद्यमान भारतीय ज्ञान प्रणालियों का पुनर्संरचनाथा, जो एक ऐसी शक्ति संरचना में अंतर्निहित था जिसने गणितीयज्ञान के स्वामित्व और वैधता को पुनर्परिभाषित किया। जीटीएसआई (GTSI) को इस व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर, यह अध्ययन औपनिवेशिक भारत में विज्ञान की अधिक संतुलित समझ में योगदान देता है, जहां सहयोग और दबाव एक साथ विद्यमान थे, और जहां स्वदेशी योगदान को मिटाना मापन की तरह ही व्यवस्थित था।